GEYS-02 SOLVED PAPER JUNE 2024
LONG ANSWER TYPE QUESTIONS
01. कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए कोशिका के विविध भागों और कार्यों का वर्णन कीजिए।
परिचय:
कोशिका (Cell) सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान (Cytology) के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका को पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) ने देखा था। कोशिकाएँ दो प्रकार की होती हैं—यूकरियोटिक (Eukaryotic) और प्रोकैरियोटिक (Prokaryotic)।
कोशिका के महत्वपूर्ण भाग
कोशिका झिल्ली (Cell Membrane)
कोशिका द्रव (Cytoplasm)
केन्द्रक (Nucleus)
माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)
राइबोसोम (Ribosomes)
गॉल्जी बॉडी (Golgi Body)
एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Endoplasmic Reticulum)
लाइसोसोम (Lysosome)
केन्द्रकिका (Nucleolus)
कोशिका के विविध भाग और उनके कार्य
कोशिका झिल्ली (Cell Membrane):
इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं।
यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है।
यह अर्ध-परगम्य (Semi-permeable) होती है और पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करती है।
कोशिका द्रव (Cytoplasm):
यह कोशिका के अंदर एक जेल जैसा तरल पदार्थ होता है।
इसमें सभी कोशिकांग (Organelles) तैरते रहते हैं।
यह कोशिका में जैव-रासायनिक क्रियाओं का केंद्र होता है।
केन्द्रक (Nucleus):
इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है।
इसमें डीएनए (DNA) और आरएनए (RNA) होता है, जो आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है।
यह कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria):
इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
यह कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है और एटीपी (ATP) का निर्माण करता है।
राइबोसोम (Ribosomes):
यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है।
यह कोशिका के अंदर मुक्त रूप से या एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होता है।
गॉल्जी बॉडी (Golgi Body):
यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों के संश्लेषण, संग्रहण और वितरण का कार्य करता है।
इसे कोशिका का "डाकघर" कहा जाता है।
एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Endoplasmic Reticulum - ER):
यह दो प्रकार का होता है:
रफ ईआर (Rough ER): इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण करता है।
स्मूथ ईआर (Smooth ER): इसमें राइबोसोम नहीं होते और यह लिपिड तथा हार्मोन संश्लेषण में मदद करता है।
लाइसोसोम (Lysosome):
इसे कोशिका का "आत्मघाती थैला" कहा जाता है।
यह अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है।
केन्द्रकिका (Nucleolus):
यह केन्द्रक के अंदर स्थित होता है।
यह राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है।
निष्कर्ष:
कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसके विभिन्न भाग मिलकर जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। कोशिका झिल्ली सुरक्षा प्रदान करती है, केन्द्रक आनुवंशिक जानकारी को नियंत्रित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, और अन्य कोशिकांग अपने-अपने कार्यों को संचालित करते हैं। इस प्रकार, कोशिका एक जटिल लेकिन संगठित संरचना है जो जीवन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
02. पेशीय तंत्र की रचना एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
परिचय
पेशीय तंत्र (Muscular System) मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो गति, संतुलन, अंगों की सुरक्षा और शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस तंत्र में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियाँ (Muscles) होती हैं, जो हड्डियों, आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती हैं। मांसपेशियाँ संकुचित (Contract) और प्रसारित (Relax) होकर शरीर की गतिविधियों को संभव बनाती हैं।
पेशीय तंत्र की रचना (Structure of Muscular System)
मानव शरीर में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं:
1. अस्थिर पेशियाँ (Skeletal Muscles)
इन्हें ऐच्छिक (Voluntary) मांसपेशियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संचालन हमारी इच्छा से होता है।
ये पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर की गति में सहायक होती हैं।
इनका निर्माण लंबी तंतुनुमा कोशिकाओं से होता है, जो पट्टिकाओं (Striations) वाली होती हैं।
उदाहरण: हाथ और पैर की मांसपेशियाँ।
2. ह्रदय पेशियाँ (Cardiac Muscles)
ये मांसपेशियाँ केवल हृदय में पाई जाती हैं और अनैच्छिक (Involuntary) होती हैं।
यह अपने आप काम करती हैं और हृदय को लगातार धड़कने में सहायता करती हैं।
इनमें विशेष प्रकार की पेशी तंतु होते हैं, जो तेज़ गति से संकुचित और प्रसारित होते हैं।
उदाहरण: हृदय की मांसपेशियाँ।
3. चिकनी पेशियाँ (Smooth Muscles)
ये अनैच्छिक (Involuntary) मांसपेशियाँ होती हैं, जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होतीं।
ये आंतरिक अंगों, रक्त वाहिकाओं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं।
इनमें पट्टिकाएँ नहीं होतीं, इसलिए इन्हें अरेखित (Non-striated) पेशियाँ भी कहा जाता है।
उदाहरण: आँतों, अमाशय और श्वासनलिका की मांसपेशियाँ।
पेशीय तंत्र के कार्य (Functions of Muscular System)
1. गति और चलन (Movement and Locomotion)
अस्थिर मांसपेशियाँ शरीर को गति प्रदान करती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना और चलना।
हड्डियों और जोड़ों के साथ मिलकर ये शरीर को आवश्यक मूवमेंट करने में सहायता करती हैं।
2. अंगों की सुरक्षा (Protection of Organs)
मांसपेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों को ढककर सुरक्षा प्रदान करती हैं।
उदाहरण: पसलियों की मांसपेशियाँ हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा देती हैं।
3. शरीर की मुद्रा बनाए रखना (Maintaining Posture)
मांसपेशियाँ शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने में मदद करती हैं।
सही मुद्रा से रीढ़ की हड्डी और अन्य जोड़ सुरक्षित रहते हैं।
4. ताप उत्पादन (Heat Production)
जब मांसपेशियाँ कार्य करती हैं तो ऊष्मा (Heat) उत्पन्न होती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।
ठंड के समय शरीर में कंपन (Shivering) मांसपेशियों की गति से उत्पन्न होता है।
5. रक्त संचार में सहायक (Helps in Blood Circulation)
ह्रदय पेशियाँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य करती हैं।
रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशियाँ रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं।
6. पाचन क्रिया में सहायता (Aids in Digestion)
आँतों और पेट की चिकनी मांसपेशियाँ भोजन को आगे बढ़ाने और पाचन में सहायता करती हैं।
पेरिस्टालिसिस (Peristalsis) नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन पाचन तंत्र में आगे बढ़ता है।
7. श्वसन में सहायक (Assists in Breathing)
डायफ्राम (Diaphragm) नामक मांसपेशी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है।
यह फेफड़ों के फैलने और संकुचित होने में मदद करती है।
8. उत्सर्जन में सहायता (Aids in Excretion)
मूत्राशय और आँतों की चिकनी मांसपेशियाँ मूत्र और मलत्याग की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं।
निष्कर्ष
पेशीय तंत्र मानव शरीर का एक अनिवार्य भाग है, जो न केवल गति और संतुलन में सहायक होता है, बल्कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा, रक्त संचार, पाचन और उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तंत्र अस्थिर, ह्रदय और चिकनी मांसपेशियों के मिलन से बनता है, जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करते हैं।
03. पाचन तंत्र की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
परिचय
पाचन तंत्र (Digestive System) मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जो क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर गुदा (Anus) पर समाप्त होती है।
पाचन तंत्र की संरचना (Structure of Digestive System)
मानव पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है:
1. पाचन नलिका (Alimentary Canal)
यह एक लंबी नलिका होती है, जो भोजन को पचाने और अवशोषित करने का कार्य करती है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं:
(i) मुख (Mouth)
भोजन पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है।
दाँत (Teeth) भोजन को चबाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदलते हैं।
लार ग्रंथियाँ (Salivary Glands) एंजाइम एमाइलेज (Amylase) का स्राव करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है।
(ii) ग्रसनी (Pharynx)
यह मुख और अन्ननली (Esophagus) के बीच स्थित एक छोटी नलिका होती है।
यह भोजन को अन्ननली में धकेलने का कार्य करती है।
(iii) अन्ननली (Esophagus)
यह एक मांसपेशीय नलिका है, जो भोजन को पेट तक पहुँचाती है।
इसमें पेरिस्टालिसिस (Peristalsis) नामक लहरदार संकुचन क्रिया होती है, जिससे भोजन नीचे की ओर बढ़ता है।
(iv) आमाशय (Stomach)
यह 'J' आकार का एक थैलीनुमा अंग है।
यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) और पेप्सिन (Pepsin) नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है।
आमाशय भोजन को 'काइम' (Chyme) नामक अर्ध-तरल रूप में परिवर्तित करता है।
(v) छोटी आंत (Small Intestine)
यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है और इसमें पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है।
इसमें तीन भाग होते हैं:
डुओडेनम (Duodenum): इसमें पित्त रस (Bile Juice) और अग्नाशयी रस (Pancreatic Juice) का मिश्रण होता है।
जेजुनम (Jejunum): यह पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है।
इलियम (Ileum): यह पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करता है।
(vi) बड़ी आंत (Large Intestine)
यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसमें जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है।
इसमें मल को संग्रहित कर गुदा (Anus) तक पहुँचाया जाता है।
(vii) गुदा (Anus)
यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ (मल) बाहर निकलता है।
2. सहायक ग्रंथियाँ (Accessory Glands)
ये ग्रंथियाँ पाचन में सहायता करती हैं:
(i) लार ग्रंथियाँ (Salivary Glands)
ये लार (Saliva) उत्पन्न करती हैं, जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को तोड़ता है।
(ii) यकृत (Liver)
यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
यह पित्त रस (Bile Juice) का निर्माण करता है, जो वसा (Fat) के पाचन में सहायता करता है।
(iii) अग्न्याशय (Pancreas)
यह इंसुलिन (Insulin) और ग्लूकागन (Glucagon) हार्मोन का स्राव करता है।
यह ट्रिप्सिन (Trypsin) और लाइपेज (Lipase) जैसे एंजाइम बनाता है, जो प्रोटीन और वसा को पचाने में मदद करते हैं।
पाचन तंत्र की क्रियाविधि (Process of Digestion)
पाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
1. ग्रहण (Ingestion)
यह प्रक्रिया भोजन के मुँह में प्रवेश करने से शुरू होती है।
दाँत भोजन को चबाते हैं और लार उसे गीला कर देती है।
2. यांत्रिक पाचन (Mechanical Digestion)
भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना और पेट में मांसपेशियों द्वारा मिलाना।
3. रासायनिक पाचन (Chemical Digestion)
इसमें विभिन्न एंजाइमों और पाचन रसों की सहायता से भोजन के बड़े अणु छोटे-छोटे घटकों में टूटते हैं।
कार्बोहाइड्रेट → ग्लूकोज (Amylase द्वारा)
प्रोटीन → अमीनो एसिड (Pepsin द्वारा)
वसा → फैटी एसिड व ग्लिसरॉल (Lipase द्वारा)
4. अवशोषण (Absorption)
छोटी आंत में पोषक तत्वों का रक्तधारा में अवशोषण होता है।
बड़ी आंत में जल और खनिजों का अवशोषण होता है।
5. परासरण (Assimilation)
अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाए जाते हैं और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
6. उत्सर्जन (Egestion)
बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है।
निष्कर्ष
पाचन तंत्र शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भोजन को ग्रहण करने, पचाने, अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। यह तंत्र कई अंगों और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जो समन्वयपूर्वक कार्य करते हैं। स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली आवश्यक है।
04. श्वसन तंत्र की रचना को समझाते हुए श्वसन तंत्र पर प्राणायाम के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
परिचय
श्वसन तंत्र (Respiratory System) मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है। यह तंत्र शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक गैसों के आदान-प्रदान को नियंत्रित करता है। श्वसन की इस प्रक्रिया को "श्वसन क्रिया" (Respiration) कहा जाता है। प्राणायाम, जो योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है।
श्वसन तंत्र की रचना (Structure of Respiratory System)
मानव श्वसन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है:
1. ऊपरी श्वसन तंत्र (Upper Respiratory Tract)
इसमें नाक, ग्रसनी और श्वासनली का ऊपरी भाग शामिल होता है।
(i) नाक (Nose)
यह श्वसन तंत्र का पहला भाग है, जहाँ से वायु प्रवेश करती है।
नाक में मौजूद बाल और श्लेष्मा झिल्ली (Mucous Membrane) धूल, कीटाणुओं और अन्य अवांछनीय कणों को रोकती है।
यहाँ वायु को गरम और आर्द्र (Humidified) किया जाता है।
(ii) ग्रसनी (Pharynx)
यह गले में स्थित एक नलिका होती है, जो नाक और श्वासनली को जोड़ती है।
यह भोजन और वायु दोनों के मार्ग के रूप में कार्य करती है।
(iii) स्वर यंत्र (Larynx)
इसे ‘वॉइस बॉक्स’ (Voice Box) भी कहते हैं, क्योंकि यह ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है।
यह फेफड़ों में वायु के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
2. निचला श्वसन तंत्र (Lower Respiratory Tract)
इसमें श्वासनली, फेफड़े और वायुकोशिकाएँ शामिल होती हैं।
(i) श्वासनली (Trachea)
यह लगभग 10-12 सेमी लंबी नलिका होती है, जो हवा को फेफड़ों तक पहुँचाती है।
इसमें उपास्थि (Cartilage) की अंगूठी जैसी संरचना होती है, जो इसे खुला रखने में मदद करती है।
(ii) ब्रोंकाई (Bronchi) और ब्रोंकिओल्स (Bronchioles)
श्वासनली दो भागों में विभाजित होकर बाएँ और दाएँ ब्रोंकाई बनाती है, जो फेफड़ों में प्रवेश करती है।
ब्रोंकाई आगे ब्रोंकिओल्स में विभाजित होकर वायुकोशिकाओं (Alveoli) तक पहुँचती हैं।
(iii) फेफड़े (Lungs)
यह श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है।
फेफड़ों में लाखों वायुकोशिकाएँ (Alveoli) होती हैं, जो गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं।
(iv) डायफ्राम (Diaphragm)
यह एक गुम्बद के आकार की पेशी होती है, जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है।
यह सिकुड़कर वायु को अंदर खींचने (Inhalation) और फैलकर वायु को बाहर निकालने (Exhalation) में मदद करता है।
श्वसन क्रिया की प्रक्रिया (Process of Respiration)
श्वसन क्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में पूरी होती है:
1. श्वास ग्रहण (Inhalation)
जब हम साँस लेते हैं, तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है और फेफड़े फैलते हैं।
हवा नाक के माध्यम से प्रवेश करके श्वासनली और ब्रोंकाई से होते हुए फेफड़ों तक पहुँचती है।
वायुकोशिकाओं (Alveoli) में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है।
2. श्वास छोड़ना (Exhalation)
जब हम साँस छोड़ते हैं, तो डायफ्राम वापस अपने स्थान पर आ जाता है और फेफड़े संकुचित हो जाते हैं।
रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोशिकाओं के माध्यम से फेफड़ों में पहुँचती है और बाहर निकल जाती है।
प्राणायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव (Effects of Pranayama on the Respiratory System)
प्राणायाम एक विशेष प्रकार की श्वसन प्रक्रिया है, जिसमें नियंत्रित रूप से गहरी और लयबद्ध साँसें ली जाती हैं। इसके श्वसन तंत्र पर अनेक लाभकारी प्रभाव होते हैं:
1. फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि
प्राणायाम से फेफड़ों की वायु ग्रहण करने और छोड़ने की क्षमता (Lung Capacity) बढ़ती है।
यह श्वसन पथ को साफ करता है और फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने योग्य बनाता है।
2. रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है
गहरी साँस लेने से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे कोशिकाएँ अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं।
इससे थकान कम होती है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है।
3. श्वसन तंत्र की सफाई
अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों से बलगम और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं।
यह अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में राहत प्रदान करता है।
4. श्वसन दर को नियंत्रित करता है
धीमी और गहरी साँसें लेने से शरीर की श्वसन दर संतुलित होती है, जिससे श्वसन तंत्र पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।
यह हृदय गति को नियंत्रित कर रक्त संचार को बेहतर बनाता है।
5. मानसिक तनाव कम करता है
प्राणायाम के दौरान गहरी साँस लेने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है।
यह तंत्रिका तंत्र को शांत करके मानसिक शांति प्रदान करता है।
6. प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
श्वसन तंत्र की शुद्धि से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत होती है।
नियमित प्राणायाम से सर्दी, खाँसी और एलर्जी की समस्या कम होती है।
निष्कर्ष
श्वसन तंत्र हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन का कार्य करता है। इसकी संरचना जटिल होते हुए भी अत्यधिक प्रभावी होती है। प्राणायाम एक प्राकृतिक उपाय है, जो श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए, नियमित रूप से प्राणायाम करने से न केवल फेफड़ों की सेहत में सुधार होता है, बल्कि संपूर्ण शरीर को भी अनेक लाभ मिलते हैं।
05. तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करें।
परिचय
तंत्रिका तंत्र (Nervous System) शरीर का एक जटिल और महत्वपूर्ण तंत्र है, जो विभिन्न अंगों के बीच संचार स्थापित करने का कार्य करता है। यह बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों को पहचानकर उचित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर बना होता है।
तंत्रिका तंत्र की रचना (Structure of Nervous System)
तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जाता है:
1. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System - CNS)
यह तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र है और इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं:
(i) मस्तिष्क (Brain)
यह खोपड़ी के अंदर स्थित शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है।
यह विचार, स्मरण, संचार, भावनाएँ और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया जाता है:
मस्तिष्क अग्रभाग (Cerebrum):
यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सोचने, बोलने, याददाश्त और संवेदी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
अनुषंग मस्तिष्क (Cerebellum):
यह संतुलन और समन्वय (Coordination) बनाए रखने का कार्य करता है।
मस्तिष्क तंत्र (Brainstem):
यह हृदय गति, श्वसन और पाचन जैसी स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
(ii) रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord)
यह मस्तिष्क से जुड़ी एक लंबी नलिका होती है, जो मेरुदंड (Vertebral Column) में स्थित होती है।
यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करती है।
2. परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System - PNS)
यह तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी भागों में तंत्रिकाओं (Nerves) का जाल बिछाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संपर्क स्थापित करता है। इसे दो भागों में बाँटा जाता है:
(i) सोमैटिक तंत्रिका तंत्र (Somatic Nervous System - SNS)
यह तंत्र शरीर की इच्छानुसार की जाने वाली क्रियाओं (जैसे चलना, दौड़ना) को नियंत्रित करता है।
यह संवेदी (Sensory) और मोटर (Motor) तंत्रिकाओं के माध्यम से कार्य करता है।
(ii) स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (Autonomic Nervous System - ANS)
यह तंत्र शरीर की अनैच्छिक (Involuntary) क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय गति, पाचन, श्वसन आदि।
इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है:
सहानुभूति तंत्रिका तंत्र (Sympathetic Nervous System):
यह शरीर को तनाव (Stress) या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है।
उदाहरण: डर लगने पर हृदय गति बढ़ना।
पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र (Parasympathetic Nervous System):
यह शरीर को शांति की स्थिति में लाता है और आंतरिक कार्यों को सामान्य बनाए रखता है।
उदाहरण: विश्राम के समय हृदय गति सामान्य होना।
तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि (Functioning of Nervous System)
तंत्रिका तंत्र सूचना के संचार और शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है:
1. संवेदी इनपुट (Sensory Input)
संवेदी तंत्रिकाएँ बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तनों (जैसे गर्मी, ठंड, दर्द, रोशनी) को पहचानती हैं।
यह जानकारी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुँचाई जाती है।
2. सूचना प्रसंस्करण (Information Processing)
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्राप्त सूचना का विश्लेषण करते हैं।
निर्णय लिया जाता है कि शरीर को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
3. मोटर आउटपुट (Motor Output)
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से आदेश भेजे जाते हैं, जिससे मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ कार्य करती हैं।
उदाहरण: गर्म वस्तु छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना।
तंत्रिका तंत्र के कार्य (Functions of Nervous System)
संवेदनशीलता (Sensitivity): यह बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तनों को महसूस करता है।
प्रतिक्रिया नियंत्रण (Response Control): यह त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जैसे रिफ्लेक्स क्रियाएँ।
संतुलन बनाए रखना (Homeostasis): यह हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर को संतुलित रखता है।
स्मृति और सीखने की प्रक्रिया (Memory and Learning): यह नई चीजें सीखने और पुरानी यादों को संग्रहीत करने में मदद करता है।
शरीर के अन्य तंत्रों का नियंत्रण (Control Over Other Systems): यह हृदय, पाचन, श्वसन, और स्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है।
निष्कर्ष
तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का जाल मिलकर पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए संतुलित आहार, योग, ध्यान और स्वस्थ जीवनशैली का पालन आवश्यक है।
SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS
01. संयोजी ऊतक से आप क्या समझते है।
संयोजी ऊतक (Connective Tissue) शरीर में विभिन्न ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने, समर्थन प्रदान करने और संरचनात्मक मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण ऊतक होता है। यह शरीर की संरचना को बनाए रखने के साथ-साथ पोषण, परिवहन, सुरक्षा और मरम्मत की प्रक्रियाओं में भी मदद करता है।
संयोजी ऊतक की विशेषताएँ:
विशेष संरचना – संयोजी ऊतक में कोशिकाएँ अधिक फैली होती हैं और इनके बीच बड़ी मात्रा में अंतःकोशिकीय पदार्थ (Extracellular Matrix) पाया जाता है।
रक्त संचार – अधिकांश संयोजी ऊतक में रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे इन्हें पोषण और ऑक्सीजन मिलता रहता है।
संरचनात्मक भूमिका – यह हड्डियों, उपास्थियों (Cartilage), रक्त और वसा ऊतक के रूप में शरीर को मजबूती प्रदान करता है।
संयोजी ऊतक के प्रकार:
संयोजी ऊतक को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी संरचना और कार्यों के आधार पर भिन्न होते हैं—
ढीला संयोजी ऊतक (Loose Connective Tissue) – यह शरीर के अंगों को लचीला सहारा देता है। उदाहरण: एरीयोलर (Areolar) और एडिपोज (Adipose) ऊतक।
घना संयोजी ऊतक (Dense Connective Tissue) – यह अधिक मजबूती और सहारा प्रदान करता है। उदाहरण: टेंडन (Tendon) और लिगामेंट (Ligament)।
विशिष्ट संयोजी ऊतक (Specialized Connective Tissue) – इसमें हड्डियाँ (Bones), उपास्थि (Cartilage) और रक्त (Blood) शामिल होते हैं।
संयोजी ऊतक के कार्य:
संरक्षण – यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है।
संरचना प्रदान करना – हड्डियाँ और उपास्थियाँ शरीर की संरचना को मजबूती देती हैं।
ऊर्जा भंडारण – वसा ऊतक (Adipose Tissue) शरीर में ऊर्जा संचित करता है।
पोषण एवं परिवहन – रक्त ऊतक (Blood Tissue) ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन को शरीर में पहुँचाता है।
प्रतिरक्षा प्रदान करना – संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएँ संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
निष्कर्ष:
संयोजी ऊतक शरीर की संरचना को बनाए रखने, पोषण प्रदान करने, ऊतकों को जोड़ने और रक्षा करने का कार्य करता है। इसके विभिन्न प्रकार शरीर के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट भूमिकाएँ निभाते हैं, जिससे यह शरीर के समुचित कार्य के लिए अनिवार्य बन जाता है।
02. हृदय की संरचना एवं कार्य।
हृदय (Heart) मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो संचार प्रणाली (Circulatory System) का केंद्र होता है। यह एक पेशीयुक्त अंग (Muscular Organ) है, जो शरीर में रक्त का संचार सुनिश्चित करता है।
हृदय की संरचना
मानव हृदय चार कक्षों (Chambers) में विभाजित होता है:
दाएँ अलिंद (Right Atrium) – यह शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है।
दाएँ निलय (Right Ventricle) – यह रक्त को फेफड़ों (Lungs) की ओर पंप करता है, जहाँ रक्त में ऑक्सीजन संचारित होता है।
बाएँ अलिंद (Left Atrium) – यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है।
बाएँ निलय (Left Ventricle) – यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है।
हृदय की दीवारें
हृदय की दीवारें तीन परतों से बनी होती हैं:
एंडोकार्डियम (Endocardium) – यह हृदय के अंदर की सबसे भीतरी परत होती है।
मायोकार्डियम (Myocardium) – यह पेशीय परत (Muscular Layer) होती है, जो हृदय को संकुचित और प्रसारित करने में मदद करती है।
पेरिकार्डियम (Pericardium) – यह बाहरी परत होती है, जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है।
हृदय वाल्व (Heart Valves)
हृदय में चार प्रमुख वाल्व होते हैं, जो रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं:
त्रिकपर्दी वाल्व (Tricuspid Valve) – दाएँ अलिंद और दाएँ निलय के बीच स्थित होता है।
माइट्रल वाल्व (Mitral Valve) – बाएँ अलिंद और बाएँ निलय के बीच स्थित होता है।
पल्मोनरी वाल्व (Pulmonary Valve) – दाएँ निलय और फेफड़ों की धमनी (Pulmonary Artery) के बीच होता है।
महाधमनी वाल्व (Aortic Valve) – बाएँ निलय और महाधमनी (Aorta) के बीच होता है।
हृदय का कार्य
हृदय का मुख्य कार्य शरीर में रक्त संचार (Blood Circulation) को बनाए रखना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
1. रक्त परिसंचरण (Blood Circulation)
सिस्टोल (Systole) – जब हृदय संकुचित होता है और रक्त को धमनियों में भेजता है।
डायास्टोल (Diastole) – जब हृदय शिथिल होता है और रक्त को प्राप्त करता है।
2. रक्त को ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित में विभाजित करना
हृदय का दायाँ भाग ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है।
हृदय का बायाँ भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है।
3. रक्तचाप (Blood Pressure) को बनाए रखना
हृदय द्वारा संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है।
4. अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना
रक्त के माध्यम से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड) फेफड़ों तक पहुँचते हैं, जहाँ से वे बाहर निकाल दिए जाते हैं।
5. पोषक तत्वों और हार्मोनों का परिवहन
हृदय रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है।
निष्कर्ष
हृदय एक पेशीयुक्त पंप की तरह कार्य करता है, जो शरीर के सभी भागों में रक्त संचार सुनिश्चित करता है। इसकी चार कक्षीय संरचना और वाल्व रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यह शरीर की संचार प्रणाली (Circulatory System) का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन को बनाए रखने में सहायक होता है।
03. यकृत की संरचना एवं कार्य।
परिचय:
यकृत (Liver) मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और ग्रंथि (Gland) है। यह पाचन तंत्र (Digestive System) का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर में चयापचय (Metabolism), विषहरण (Detoxification), और पाचन में सहायक होता है।
यकृत की संरचना
1. स्थिति और आकार:
यकृत पेट के ऊपरी दाएँ भाग में स्थित होता है।
इसका वजन लगभग 1.4 से 1.6 किलोग्राम होता है।
यह लाल-भूरे रंग का एक त्रिकोणीय अंग होता है।
2. लोब (Lobes):
यकृत दो मुख्य लोब में विभाजित होता है:
दायाँ लोब (Right Lobe) – यह बड़ा होता है।
बायाँ लोब (Left Lobe) – यह छोटा होता है।
3. हेक्सागोनल लोब्यूल्स (Lobules):
यकृत छोटे-छोटे इकाइयों (Lobules) से बना होता है, जो हेक्सागोनल आकार की संरचनाएँ होती हैं। प्रत्येक लोब्यूल में यकृत कोशिकाएँ (Hepatocytes) होती हैं, जो विभिन्न जैविक क्रियाएँ संचालित करती हैं।
4. रक्त संचार (Blood Supply):
यकृत को रक्त की आपूर्ति दो प्रमुख स्रोतों से होती है:
यकृत धमनी (Hepatic Artery): यह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है।
पोर्टल शिरा (Portal Vein): यह पाचन तंत्र से पोषक तत्वों युक्त रक्त लाती है।
5. पित्ताशय (Gallbladder):
यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय (Gallbladder) में यकृत द्वारा निर्मित पित्त (Bile) संचित रहता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है।
यकृत के कार्य
यकृत शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जो इसे शरीर का एक प्रमुख जैव-रासायनिक केंद्र बनाते हैं।
1. पाचन में सहायता:
यकृत पित्त (Bile) नामक द्रव का स्राव करता है, जो वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है।
2. चयापचय (Metabolism) को नियंत्रित करना:
कार्बोहाइड्रेट चयापचय: यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहीत करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर रक्त में छोड़ता है।
प्रोटीन चयापचय: यकृत अमीनो एसिड को संसाधित करता है और यूरिया का निर्माण करता है, जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है।
वसा चयापचय: यकृत में वसा का अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है।
3. विषहरण (Detoxification):
यकृत हानिकारक पदार्थों (जैसे अल्कोहल, ड्रग्स और विषैले तत्वों) को निष्क्रिय कर शरीर से बाहर निकालता है।
4. प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना:
यकृत में कुप्फर कोशिकाएँ (Kupffer Cells) होती हैं, जो बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट कर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं।
5. रक्त संचारण एवं थक्के बनाना:
यकृत रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य कारकों का उत्पादन करता है।
6. पोषक तत्वों का भंडारण:
यकृत में विटामिन (A, D, B12, K) और खनिज (आयरन, तांबा) संचित होते हैं, जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।
7. हार्मोन संतुलन बनाए रखना:
यकृत शरीर में थायरॉइड, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।
निष्कर्ष
यकृत मानव शरीर का एक आवश्यक अंग है, जो पाचन, चयापचय, विषहरण और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसकी संरचना जटिल होती है और यह कई महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देता है। स्वस्थ यकृत के लिए संतुलित आहार, कम वसा वाला भोजन, नियमित व्यायाम और अल्कोहल से बचाव आवश्यक होता है।
04. अस्थि संस्थान पर योग का प्रभाव।
परिचय:
अस्थि संस्थान (Skeletal System) मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर को संरचना, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह हड्डियों (Bones), उपास्थि (Cartilage), जोड़ (Joints) और स्नायुबंधन (Ligaments) से मिलकर बना होता है। योग एक प्राचीन भारतीय विधा है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए उपयोगी होती है। योगाभ्यास अस्थि संस्थान को मजबूत बनाने, लचीला बनाए रखने और हड्डी संबंधी विकारों से बचाने में सहायक होता है।
योग का अस्थि संस्थान पर प्रभाव
1. हड्डियों की मजबूती में सहायता
योगाभ्यास से शरीर में कैल्शियम और विटामिन D का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं।
भार-सहायक योगासन (Weight-bearing Asanas) जैसे वीरभद्रासन (Warrior Pose), त्रिकोणासन (Triangle Pose) हड्डियों की घनत्व (Bone Density) को बनाए रखते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) के खतरे को कम करते हैं।
2. जोड़ (Joints) को लचीला बनाना
योगाभ्यास से जोड़ों की गति बढ़ती है और वे लचीले बनते हैं।
सुखासन (Easy Pose), भुजंगासन (Cobra Pose), वज्रासन (Thunderbolt Pose) जैसे आसन जोड़ों में चिकनाई बनाए रखते हैं और गठिया (Arthritis) से राहत दिलाते हैं।
3. रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना
रीढ़ की हड्डी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, जो पूरे शरीर को सहारा देती है।
भुजंगासन (Cobra Pose), अर्धमत्स्येन्द्रासन (Half Spinal Twist Pose) रीढ़ की लचीलेपन को बढ़ाते हैं और पीठ दर्द को कम करते हैं।
4. संतुलन और मुद्रा सुधारना
योगाभ्यास से शरीर का संतुलन और मुद्रा (Posture) सुधरती है, जिससे हड्डियों और जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है।
ताड़ासन (Mountain Pose), वृक्षासन (Tree Pose) संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं।
5. हड्डियों की चोटों और फ्रैक्चर के खतरे को कम करना
योग से मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे हड्डियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होता है।
योग शरीर की सहनशक्ति (Endurance) बढ़ाता है, जिससे गिरने और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है।
6. रक्त संचार में सुधार
योगासन करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हड्डियों को अधिक पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहती हैं।
अधोमुखश्वानासन (Downward Dog Pose), पश्चिमोत्तानासन (Seated Forward Bend) रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं।
योग के माध्यम से अस्थि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुझाव
नियमित योगाभ्यास करें – हड्डियों की मजबूती के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग करें।
संतुलित आहार लें – कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें।
ध्यान (Meditation) और प्राणायाम करें – यह मानसिक तनाव को कम करता है, जिससे हड्डियों पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
अत्यधिक कठोर व्यायाम से बचें – हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए योग करते समय सही तकनीक का पालन करें।
निष्कर्ष
योगाभ्यास अस्थि संस्थान को मजबूत करने, जोड़ों को लचीला बनाए रखने, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने और हड्डी संबंधी विकारों से बचाने में सहायक होता है। नियमित योगाभ्यास और संतुलित आहार अपनाकर हड्डियों की मजबूती और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
05. रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए।
परिचय
रक्त (Blood) शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक (Connective Tissue) है, जो संचार प्रणाली (Circulatory System) का हिस्सा है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है।
रक्त के प्रमुख कार्य
1. गैसों का परिवहन (Transport of Gases)
लाल रक्त कोशिकाएँ (Red Blood Cells - RBC) में उपस्थित हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाकर बाहर निकालने में मदद करता है।
2. पोषक तत्वों का परिवहन (Transport of Nutrients)
रक्त पाचन तंत्र (Digestive System) से अवशोषित ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और खनिज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाता है।
3. अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन (Excretion of Waste Products)
कोशिकाओं से उत्पन्न मूत्रिया (Urea), यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आदि को गुर्दों (Kidneys) तक पहुँचाता है, जहाँ से ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं।
4. शरीर के तापमान का नियंत्रण (Regulation of Body Temperature)
रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ऊष्मा (Heat) को समान रूप से वितरित करता है, जिससे शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है।
5. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना (Immunity Boosting)
श्वेत रक्त कोशिकाएँ (White Blood Cells - WBC) शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों से बचाती हैं।
प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी (Antibodies) और ल्यूकोसाइट्स (Leukocytes) संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
6. हार्मोन का परिवहन (Transport of Hormones)
रक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों (Endocrine Glands) से स्रावित हार्मोन को शरीर के लक्ष्य अंगों (Target Organs) तक पहुँचाता है, जिससे विभिन्न जैविक क्रियाएँ नियंत्रित होती हैं।
7. रक्त का थक्का बनाना (Blood Clotting)
जब शरीर में किसी स्थान पर चोट लगती है, तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स (Platelets) और फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen) रक्त का थक्का (Clot) बनाकर अधिक रक्तस्राव (Bleeding) को रोकते हैं।
8. शरीर के पीएच (pH) संतुलन को बनाए रखना
रक्त में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन (HCO₃⁻) शरीर के अम्ल-क्षार संतुलन (Acid-Base Balance) को बनाए रखते हैं, जिससे शरीर की जैविक प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से चलती हैं।
9. जल संतुलन बनाए रखना (Regulation of Water Balance)
रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं के अंदर और बाहर जल के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर में जल संतुलन बना रहता है।
10. शरीर के विभिन्न भागों में संचारण (Circulation in the Body)
हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है, जिससे सभी कोशिकाएँ क्रियाशील बनी रहती हैं।
निष्कर्ष
रक्त शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन को संचारित करने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, रोगों से लड़ने, तापमान संतुलन बनाए रखने और रक्तस्राव रोकने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। स्वस्थ रक्त संचार प्रणाली (Healthy Circulatory System) संपूर्ण शारीरिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।
06. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं।
परिचय
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System - CNS) शरीर की प्रमुख नियंत्रण प्रणाली है, जो सभी संवेदी (Sensory) और गतिज (Motor) कार्यों को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिका तंत्र (Nervous System) का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर की सभी गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है:
1. मस्तिष्क (Brain)
मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और शक्तिशाली अंग है, जो विचार, स्मृति, भावनाएँ और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह तीन मुख्य भागों में विभाजित होता है:
(क) अग्र मस्तिष्क (Forebrain)
इसमें मस्तिष्कीय प्रांतस्था (Cerebral Cortex), थैलेमस (Thalamus) और हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) शामिल होते हैं।
यह संज्ञानात्मक कार्यों (Cognitive Functions) जैसे विचार, निर्णय, स्मरण शक्ति और भावनाओं को नियंत्रित करता है।
(ख) मध्य मस्तिष्क (Midbrain)
यह श्रवण (Hearing) और दृष्टि (Vision) से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है।
यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संदेशों का संचार करता है।
(ग) पश्च मस्तिष्क (Hindbrain)
इसमें सेरिबेलम (Cerebellum), पोंस (Pons) और मेडुला ऑब्लोंगाटा (Medulla Oblongata) शामिल होते हैं।
यह संतुलन, समन्वय, हृदय गति और श्वसन दर को नियंत्रित करता है।
2. रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord)
यह एक लंबी, नलिका के आकार की संरचना होती है, जो मस्तिष्क को पूरे शरीर से जोड़ती है।
यह शरीर के विभिन्न भागों से संवेदी और गतिज सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करती है।
यह कुछ त्वरित क्रियाओं (Reflex Actions) को बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के नियंत्रित करती है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य
1. सूचना ग्रहण करना (Receiving Information)
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदी सूचनाएँ ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता है।
2. निर्णय लेना और प्रतिक्रियाएँ देना (Decision Making and Response)
मस्तिष्क सभी संवेदनाओं का विश्लेषण कर उचित प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है।
यह सोचने, याद रखने और निर्णय लेने में मदद करता है।
3. शरीर की गतियों को नियंत्रित करना (Controlling Movements)
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों और अंगों को संकेत भेजकर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
4. संतुलन और समन्वय बनाए रखना (Maintaining Balance and Coordination)
सेरिबेलम (Cerebellum) शरीर की गति, संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है।
5. शरीर की स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करना (Regulating Involuntary Actions)
हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन और रक्तचाप जैसी स्वायत्त (Autonomic) क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
6. रिफ्लेक्स क्रियाएँ (Reflex Actions) संचालित करना
रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के त्वरित प्रतिक्रियाएँ (Reflex Actions) उत्पन्न कर सकती है, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटा लेना।
निष्कर्ष
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तंत्र है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है और सभी संवेदी एवं गतिज कार्यों का संचालन करता है। इसके बिना शरीर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। स्वस्थ जीवन के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सुचारु रूप से कार्य करना आवश्यक है।
07. शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइये।
परिचय
मूत्र निर्माण (Urine Formation) एक जैविक प्रक्रिया है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में मदद करती है। यह प्रक्रिया गुर्दों (Kidneys) में होती है और यह शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में संपन्न होती है: गुच्छिक निस्यंदन (Glomerular Filtration), पुनः अवशोषण (Reabsorption) और स्रावण (Secretion)।
मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
1. गुच्छिक निस्यंदन (Glomerular Filtration)
यह प्रक्रिया गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन (Nephron) में होती है।
रक्त, वृक्क धमनी (Renal Artery) के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है और वहाँ मौजूद गुच्छिका (Glomerulus) नामक केशिका जालिका में निस्यंदन (Filtration) होता है।
उच्च रक्तचाप के कारण, पानी, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड, लवण और अन्य छोटे अणु बोमैन संपुट (Bowman’s Capsule) में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि बड़े अणु (जैसे प्रोटीन और रक्त कोशिकाएँ) रक्त प्रवाह में ही बने रहते हैं।
इस चरण में बनने वाले तरल को गुच्छिक निस्यंद (Glomerular Filtrate) कहा जाता है।
2. पुनः अवशोषण (Reabsorption)
यह प्रक्रिया नेफ्रॉन की घुमावदार नलिकाओं (Renal Tubules) में होती है।
गुच्छिका से निस्यंदित पदार्थों में से आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जल और लवण पुनः रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं।
पुनः अवशोषण मुख्य रूप से हेनले का लूप (Loop of Henle) और डिस्टल नलिका (Distal Tubule) में होता है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर में जल और लवणों का संतुलन बनाए रखना है।
3. स्रावण (Secretion)
यह अंतिम प्रक्रिया है, जिसमें नेफ्रॉन की नलिकाओं द्वारा अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन (H⁺), पोटैशियम आयन (K⁺), क्रिएटिनिन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ सक्रिय रूप से मूत्र नलिका (Urinary Tubule) में प्रवाहित किए जाते हैं।
यह शरीर के अम्ल-क्षार संतुलन (Acid-Base Balance) को बनाए रखने में मदद करता है।
इस प्रक्रिया के बाद, अंतिम रूप से तैयार मूत्र एकत्रीकरण नलिका (Collecting Duct) में एकत्र होता है।
मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया
एकत्रीकरण नलिका से मूत्र वृक्क वाहिनी (Ureter) के माध्यम से मूत्राशय (Urinary Bladder) में जाता है।
जब मूत्राशय भर जाता है, तो मस्तिष्क को संकेत भेजा जाता है, जिससे मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है।
मूत्र मूत्रमार्ग (Urethra) के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है।
निष्कर्ष
मूत्र निर्माण की प्रक्रिया गुर्दों में तीन चरणों—गुच्छिक निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रावण—के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने और जल तथा लवण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुर्दों के सही ढंग से कार्य करने से शरीर का आंतरिक संतुलन (Homeostasis) बना रहता है और विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
08. आंख की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें।
परिचय
आंख (Eye) मानव शरीर की एक जटिल एवं संवेदनशील इंद्रिय है, जो प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क को दृश्य संकेत भेजने का कार्य करती है। यह प्रकाशीय तंत्र (Optical System) का हिस्सा है और हमें रंग, आकार, दूरी तथा गति को समझने में मदद करती है।
आंख की संरचना
आंख मुख्य रूप से तीन परतों और विभिन्न आंतरिक संरचनाओं से बनी होती है:
1. बाहरी परत (Outer Layer)
यह परत आंख की सुरक्षा करती है और प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देती है। इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं:
कॉर्निया (Cornea):
यह आंख का सबसे बाहरी, पारदर्शी एवं गोलाकार भाग होता है।
यह प्रकाश को अपवर्तित (Refract) करके आंख के अंदर भेजता है।
इसमें कोई रक्त वाहिकाएँ नहीं होतीं, लेकिन यह आँसुओं और ऑक्सीजन से पोषण प्राप्त करता है।
श्वेतपटल (Sclera):
यह आंख का सफेद, कठोर एवं बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है।
यह आंख को आकार और मजबूती प्रदान करता है।
2. मध्य परत (Middle Layer) – संवहनी परत (Vascular Layer)
यह परत आंख को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं:
रतौंधी झिल्ली (Choroid):
यह रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है और रेटिना को पोषण देती है।
आईरिस (Iris):
यह आंख के रंगीन भाग के रूप में दिखता है और रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है।
पुतली (Pupil):
यह आंख के केंद्र में एक छोटा छिद्र होता है, जो रोशनी के प्रवेश को नियंत्रित करता है।
यह कम रोशनी में फैलता (Dilate) और तेज रोशनी में सिकुड़ता (Constrict) है।
3. आंतरिक परत (Inner Layer) – रेटिना (Retina)
यह आंख की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जिसमें छड़ (Rods) और शंकु (Cones) नामक प्रकाश-संवेदनशील कोशिकाएँ होती हैं।
छड़ कोशिकाएँ (Rods): कम रोशनी में देखने में सहायक होती हैं।
शंकु कोशिकाएँ (Cones): रंग पहचानने और दिन में देखने में मदद करती हैं।
रेटिना प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर ऑप्टिक तंत्रिका (Optic Nerve) के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचाती है।
अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएँ
काचाभ शरीर (Vitreous Body): यह एक जैली जैसा पदार्थ होता है, जो आंख के अंदरूनी भाग को भरता है और इसे स्थिरता प्रदान करता है।
लेंस (Lens):
यह पारदर्शी और लचीला होता है, जो प्रकाश को अपवर्तित करके उसे रेटिना पर केंद्रित करता है।
यह पास और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
ऑप्टिक तंत्रिका (Optic Nerve): यह रेटिना से संवेदी जानकारी को मस्तिष्क तक पहुँचाती है, जिससे हम देख पाते हैं।
आंख के कार्य
1. प्रकाश ग्रहण करना (Light Reception)
कॉर्निया और लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं और उसे रेटिना पर केंद्रित करते हैं।
2. इमेज निर्माण (Image Formation)
लेंस प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर एक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
3. विद्युत संकेतों में परिवर्तन (Conversion to Electrical Signals)
रेटिना की छड़ और शंकु कोशिकाएँ प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं।
4. मस्तिष्क तक सूचना संचार (Transmission to Brain)
ऑप्टिक तंत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था (Visual Cortex) तक पहुँचाती है, जहाँ छवि को सही रूप में पहचाना जाता है।
5. रोशनी की मात्रा का नियंत्रण (Light Adjustment)
आईरिस और पुतली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जिससे तेज रोशनी में आंख को नुकसान नहीं होता और कम रोशनी में देखने की क्षमता बनी रहती है।
6. निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना (Focusing on Near and Distant Objects)
लेंस अपनी मोटाई को बदलकर समायोजन (Accommodation) करता है, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
निष्कर्ष
आंख एक जटिल और संवेदनशील इंद्रिय है, जो प्रकाश को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक संप्रेषित करने का कार्य करती है। इसकी संरचना में कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका और अन्य सहायक भाग शामिल होते हैं। यह हमें रंग, आकार और गहराई का अनुभव करने में सहायता करती है। स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए उचित पोषण, स्वच्छता और नियमित नेत्र जांच आवश्यक है।

.png)

%20(1200%20x%20675%20px)%20(3).jpg)




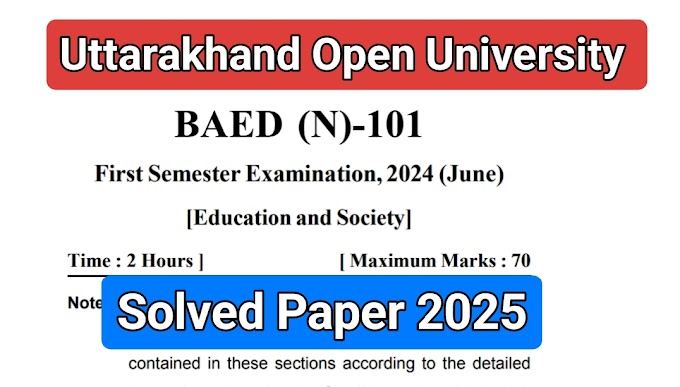
.png)



